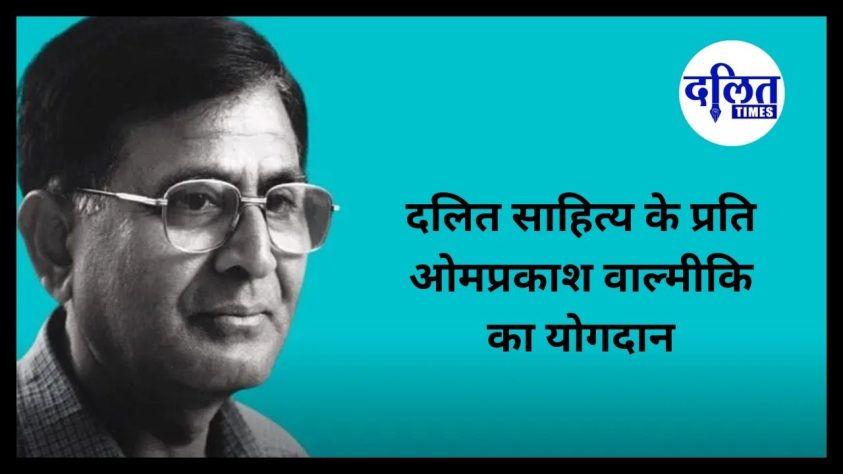2019 में सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की नगरपालिकाएँ और पंचायतें स्वयं 54,098 सफाई कर्मचारियों को मैला ढोने के लिए नियुक्त कर रही थीं। सरकारें इस समस्या को केवल एक प्रशासनिक मुद्दा मानती हैं, जबकि यह एक गंभीर मानवीय संकट है।
सफाई का कार्य किसी भी समाज के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए अनिवार्य है, लेकिन जब यह कार्य कुछ चुनिंदा लोगों पर थोपा जाए और इसे उनकी पहचान से जोड़ दिया जाए, तो यह एक गहरी सामाजिक अन्याय की ओर संकेत करता है। भारत में मैला ढोने की प्रथा न केवल एक अमानवीय कार्य है, बल्कि यह जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का जीता-जागता प्रमाण भी है।
संविधान की प्रस्तावना भारत को एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने वाला लोकतंत्र बनाने की बात कहती है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करने की गारंटी देता है, और अनुच्छेद 19(1) (ग) व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके बावजूद, भारत में मैला ढोना एक जाति विशेष पर थोपे गए पेशे के रूप में जारी है। यह न केवल संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक असमानता को स्थायी बनाए रखने का एक जरिया भी है।
वर्षों से, सरकारों ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए, लेकिन कानूनी निषेध और वास्तविकता के बीच गहरी खाई बनी हुई है। आधुनिक तकनीक और मशीनों के युग में भी, हज़ारों लोग नंगे हाथों और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने को मजबूर हैं। यह मजबूरी सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक विफलताओं का परिणाम है।
31 जुलाई 2024 को संसद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री श्री रामदास अठावले ने एक प्रतिउत्तर में बताया कि 2019 से 2023 के बीच भारत में 377 लोग सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए मारे गए। यह संख्या केवल आधिकारिक रूप से दर्ज मौतों को दर्शाती है। हकीकत में, यह संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि कई मौतें बिना किसी दस्तावेज़ीकरण के गुम हो जाती हैं।
यह भी पढ़ें : बजट निर्माण प्रक्रिया पर उठें सवाल: AAP की टीम में नहीं दलित, न आदिवासी, न पिछड़ा
इसके पीछे प्रशासनिक उदासीनता और समाज की उपेक्षा दोनों जिम्मेदार हैं। यह केवल आकड़ों का सवाल नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन का प्रश्न है, जिनकी मृत्यु को एक सामान्य घटना मानकर भुला दिया जाता है। इसी प्रतिउत्तर में यह भी बताया गया कि भारत में 58,098 लोग आधिकारिक रूप से मैला ढोने के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है, क्योंकि यह पेशा एक जाति विशेष के लिए जबरन निर्धारित कर दिया गया है।
भारतीय समाज की विफलता
————————————-
भारत को गणतंत्र बने 70 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव अब भी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ है। राष्ट निर्माता बाबासाहेब अंबेडकर ने जिस समानता और न्याय पर आधारित समाज का सपना देखा था, वह आज भी अधूरा है।
संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, लेकिन व्यावसायिक स्वतंत्रता केवल कागज़ों तक सीमित रह गई है। वाल्मीकि समाज और अन्य वंचित समुदायों को सफाई के कार्यों तक सीमित कर दिया गया है, जिससे उनकी अन्य व्यवसायों में भागीदारी लगभग नगण्य है।
“From Shadows to Spotlight: Unveiling the Saga of Manual Scavenging in India” Rupkatha journal नामक शोध-पत्र के अनुसार, आज भी मैला ढोने का कार्य पूरी तरह से जाति-आधारित है, और इसे केवल एक समुदाय पर जबरन थोपा गया है।
साहित्य में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने एक लेख में लिखा “तिहवार ही तुम्हारी म्युनिसिपालिटी मिली है।” यानी त्योहारों के समय लोग केवल अपने घरों की सफाई करते हैं, जबकि सार्वजनिक सफाई की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों पर डाल दी जाती है। बदले में, उन्हें न्यूनतम वेतन और अमानवीय परिस्थितियाँ दी जाती हैं।
एकाधिकार (Monopoly) के बावजूद न्यूनतम अधिकार
आर्थिक दृष्टि से देखें तो, किसी भी व्यवसाय में यदि एक वर्ग का एकाधिकार (monopoly) होता है, तो वह अपनी शर्तों पर मेहनताना तय कर सकता है। लेकिन सफाई कर्मचारियों के मामले में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि:

1. वे अशिक्षा और आर्थिक असुरक्षा के कारण अपने अधिकारों की माँग करने में असमर्थ हैं।
2. समाज ने इस कार्य को केवल उनकी नियति मान लिया है।
3. राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में उनकी भागीदारी नगण्य है।
यह भी पढ़ें : दिल्ली चुनाव: आरक्षित सीटों की जंग और दलित वोटों का खेल, इस बार दलित वोटर किसके साथ?
राजनीतिक विफलता
कानूनी निषेध, लेकिन अमल में उदासीनता
भारत में मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन वे प्रभावी रूप से लागू नहीं किए गए।
The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 ने मैला ढोने और सूखे शौचालयों के निर्माण को अवैध घोषित किया।
2013 का नया कानून सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास की बात करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका प्रभाव न के बराबर है।
2019 में सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की नगरपालिकाएँ और पंचायतें स्वयं 54,098 सफाई कर्मचारियों को मैला ढोने के लिए नियुक्त कर रही थीं। सरकारें इस समस्या को केवल एक प्रशासनिक मुद्दा मानती हैं, जबकि यह एक गंभीर मानवीय संकट है।
राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका
2007-2012 के दौरान, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को जाति-आधारित एकाधिकार से मुक्त करने का प्रयास किया। सभी जातियों के लोगों को सफाईकर्मी बनने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई। लेकिन अन्य राज्यों में सरकारें अब भी सफाई कार्य को एक जाति तक सीमित रखती हैं।
सफाई कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियों की कमी सरकारों की जातिवादी मानसिकता को उजागर करती है।
नीतिगत विफलता :
गणतंत्र के 70 दशकों के बाद भी मैला ढोने का कार्य एक ही जाति तक सीमित रहना सरकार की नीतिगत विफलता का प्रमाण है। सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए कोई ठोस योजनाएँ नहीं बनाई गईं। जो योजनाएँ बनीं, वे आधे-अधूरे मन और अपर्याप्त संसाधनों के साथ लागू की गईं।
सरकारों को चाहिए कि वे सफाई कर्मचारियों के कौशल विकास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएँ।
1. सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई।
2. कौशल विकास और शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए।
3. सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कोई ठोस अभियान नहीं चलाया गया।
यह भी पढ़ें : BHU में इस तरह मनाई गई संत गुरु रविदास जी की जयंती, रविदास के शिक्षाओं पर छात्रों ने बनाई चित्रकला !
साथ ही, समाज को यह समझना होगा कि राजनीतिक पहचान के बिना किसी भी समुदाय की समस्याओं को हल्के में लिया जाता है। इसलिए, सफाई कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपने सशक्त राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण करें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें।राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में सफाई कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाई जाए।
निष्कर्ष :
मैला ढोने की अमानवीय प्रथा भारतीय समाज, सरकारों और नीतियों की सामूहिक विफलता को दर्शाती है। यह केवल एक व्यावसायिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय और मानवीय गरिमा का प्रश्न है। जब तक इस समुदाय को शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक भारतीय लोकतंत्र की नींव अधूरी ही रहेगी।
अब समय आ गया है कि सरकारें और समाज सफाई कर्मचारियों को केवल सफाईकर्मी नहीं, बल्कि एक समान अधिकार वाला नागरिक समझें। तभी भारत सच में स्वतंत्र और समतामूलक समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।
दीपशिखा इन्द्रा
नमो बुद्धाय जय भीम
(इस लेख में हमने किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया है। लेख की पूरी जिम्मेदारी लेखक की है। )